৵ৌа§∞ а§Ха•З ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч а§Ха§єа§Ња§В ১৕ৌ 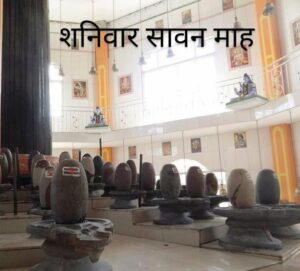
а§Ха•На§ѓа•Ла§В а§єа•И, а§За§Єа§Ха•А а§Єа§Ѓа•Аа§Ха•На§Ја§Њ а§Ха•А а§Ьа§Њ а§∞а§єа•А а§єа•Иа•§
৵а•З৶ৌа§Ща•На§Ч а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ-
а§За§Є ৮ৌু а§Ха•З а•© а§Ча•На§∞৮а•Н৕ а§єа•Иа§В-а§Ла§Ха•Н, а§ѓа§Ња§Ьа•Ба§Ј, а§Е৕а§∞а•На§µа§£а•§ а§Ла§Ха•Н ১৕ৌ а§ѓа§Ьа•Ба§∞а•Н৵а•З৶ а§Ѓа•За§В а§≤а§ња§Ца§Њ а§єа•И а§Ха§њ ৵а•З৶ а§ѓа§Ьа•На§Ю а§Ха•З а§≤а§ња§П а§єа•Иа§В, а§ѓа§Ьа•На§Ю а§Ха§Ња§≤ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Е১а§Г а§Ха§Ња§≤ ৮ড়а§∞а•На§Іа§Ња§∞а§£ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ а§єа•Иа•§ ৵а•З৶ৌ а§єа§њ а§ѓа§Ьа•На§Юа§Ња§∞а•Н৕ুа§≠ড়৙а•На§∞৵а•Г১а•Н১ৌа§Г, а§Ха§Ња§≤ৌ৮а•Б৙а•Ва§∞а•Н৵а•На§ѓа§Њ ৵ড়৺ড়১ৌ৴а•На§Ъ а§ѓа§Ьа•На§Юа§Ња§Га•§ ১৪а•Нুৌ৶ড়৶а§В а§Ха§Ња§≤৵ড়৲ৌ৮৴ৌ৪а•Н১а•На§∞а§В, а§ѓа•Л а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣа§В ৵а•З৶ а§Є ৵а•З৶ а§ѓа§Ьа•На§Юৌ৮а•На•• (а§Ла§Ха•Н а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ, а•©а•ђ, а§ѓа§Ња§Ьа•Ба§Ј а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ, а•©) а§Ла§Ха•Н а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ а§Ѓа•За§В а§Ха§Ња§≤ а§Ха•А а§Ча§£а§®а§Њ а§єа•И а§Ьа§ња§Єа§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а•Іа•ѓ ৵а§∞а•На§Ј а§Ха§Њ а§ѓа•Ба§Ч а§єа•Л১ৌ а§єа•И, а§За§Єа§Ѓа•За§В а•Ђ ৵а§∞а•На§Ј а§Єа§В৵১а•На§Єа§∞ а§єа•Иа§В, а§Е৮а•На§ѓ а•Іа•™ ৵а§∞а•На§Ј а§Е৮а•На§ѓ а•™ ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•З а§єа•Иа§В-৙а§∞ড়৵১а•На§Єа§∞, а§З৶ৌ৵১а•На§Єа§∞, а§Е৮а•Б৵১а•На§Єа§∞, а§З৶а•Н৵১а•На§Єа§∞а•§ ৙а§∞ а§Ха•М৮ а§Єа§Њ а§ѓа§Ьа•На§Ю а§Ха§ђ а§Ха§ња§ѓа§Њ а§Ьа§Ња§ѓ а§ѓа§є а§Ха§єа•Аа§В ৮৺а•Аа§В а§≤а§ња§Ца§Њ а§єа•Иа•§ а§ѓа§Ња§Ьа•Ба§Ј а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ а§Ѓа•За§В а§ѓа§Ьа•На§Ю а§Ха§Ња§≤ а§Ха•З а§Єа§Ва§Ха•Нৣড়৙а•Н১ а§Йа§≤а•На§≤а•За§Ц а§єа•Иа§В-৴а•На§≤а•Ла§Х а•©а•®-а•©а•™ а§Ѓа•За§В ৮а§Ха•Нৣ১а•На§∞ ৶а•З৵১ৌа§Уа§В а§Ха•А а§Єа•Ва§Ъа•А ৶а•З а§Ха§∞ ৴а•На§≤а•Ла§Х а•©а•Ђ а§Ѓа•За§В а§Ха§єа§Њ а§єа•И а§Ха§њ а§З৮ ৶а•З৵а•Ла§В а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§ѓа§Ьа•На§Ю а§єа•Л৮ৌ а§Ъа§Ња§єа§ња§Па•§ ৮а§Ха•Нৣ১а•На§∞ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ ৮ৌু а§∞а§Ц৮а•З а§Ха§Њ а§≠а•А ৵ড়৲ৌ৮ а§єа•И, ৙а§∞ а§Ха§ња§Є ৮а§Ха•Нৣ১а•На§∞ а§ѓа§Њ а§Йа§Єа§Ха•З ৙ৌ৶ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§Ха•На§ѓа§Њ ৮ৌু а§єа•Ла§Ча§Њ, ৵৺ (а§Е৵а§Ха§єа§°а§Њ а§Ъа§Ха•На§∞) ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ ৴а•На§≤а•Ла§Х а•©а•ђ а§Ѓа•За§В а§Йа§Ча•На§∞ ১৕ৌ а§Ха•На§∞а•Ва§∞ ৮а§Ха•Нৣ১а•На§∞а•Ла§В а§Ха•З ৮ৌু а§єа•Иа§Ва•§ ৴а•На§≤а•Ла§Х а•©а•Ѓ а§Ѓа•За§В а§Ѓа•Ба§єа•Ва§∞а•Н১а•Н১ ুৌ৮, ১৕ৌ а•™а•® а§Ѓа•За§В а§Й৙ৃа•Ба§Ха•Н১ а§Єа§Ѓа§ѓ а§Еа§∞а•Н৕ а§Ѓа•За§В а§Ѓа•Ба§єа•Ва§∞а•Н১а•Н১ а§Йа§≤а•На§≤а•За§Ц а§єа•Иа•§ а§Ж৕а§∞а•На§µа§£ а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ а§Ѓа•За§В ৵ড়а§≠ড়৮а•Н৮ а§Ха§Ња§Ѓа•Ла§В а§Ха•З а§≤а§ња§П ৴а•Ба§≠-а§Е৴а•Ба§≠ а§Ѓа•Ба§єа•Ва§∞а•Н১а•Н১ ১৕ৌ ৙а§Юа•На§Ъа§Ња§Ща•На§Ч а§Ха•З а•Ђ а§Еа§Ва§Ч ৶ড়ৃа•З а§єа•Иа§В-১ড়৕ড়, ৵ৌа§∞, ৮а§Ха•Нৣ১а•На§∞, а§ѓа•Ла§Ч ১৕ৌ а§Ха§∞а§£а•§ а§З৮ а§Єа§≠а•А а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§Ѓа•Ба§єа•Ва§∞а•Н১а•Н১ а§Ха•З ৴а•Ба§≠ а§єа•Л৮а•З а§Ха§Њ ৮ড়а§∞а•На§£а§ѓ ৶ড়ৃৌ а§єа•Иа•§ ৴а•На§≤а•Ла§Х а•ѓа•© а§Ѓа•За§В ৵ৌа§∞ а§Ха§Њ ৵а§∞а•Н১ুৌ৮ а§Ха•На§∞а§Ѓ ৶ড়ৃৌ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•Иа•§ а§Йа§Єа§Ха•З ৐ৌ৶ а§Ха§ња§Є ৵ৌа§∞ а§Ѓа•За§В а§Ха•М৮ а§Єа§Њ а§Ха§Ња§Ѓ а§Й৙ৃа•Ба§Ха•Н১ а§єа•И, а§ѓа§є а§Ха§єа§Њ а§єа•Иа•§ ১а•А৮а•Ла§В ৵а•З৶ৌа§Ща•На§Ч а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ а§Ѓа§ња§≤ а§Ха§∞ а§ѓа§Ьа•На§Ю а§Єа§Ѓа§ѓ а§Ха•З а§Й৶а•Н৶а•З৴а•На§ѓ а§Єа•З ৵а•З৶ৌа§Ща•На§Ч а§єа•Иа§В а§Хড়৮а•Н১а•Б а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ а§Ха•Л ৵а•З৶ а§Ха§Њ ৮а•З১а•На§∞ а§Ха§єа§Њ а§єа•И, а§За§Є а§Еа§∞а•Н৕ а§Ѓа•За§В ৵а•З৶ а§Ха§Њ а§Ьа•На§Юৌ৮ а§З৮৪а•З ৮৺а•Аа§В а§єа•Л а§∞а§єа§Њ а§єа•Иа•§ ৵а•З৶ а§Ха•З а•≠ а§≤а•Ла§Ха•Ла§В а§Ха•А ুৌ৙ ৙а•Ба§∞а§Ња§£а•Ла§В а§Ха•З а§≠а•Б৵৮ а§Ха•Ла§Ј а§Ѓа•За§В а§єа•Иа•§ ৙а•Ма§∞а§Ња§£а§ња§Х ুৌ৙а•Ла§В а§Ха§Њ ুৌ৮ а§Ьа•И৮ а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ а§Ѓа•За§В а§єа•И, ১৕ৌ а§З৮ ৮ৌুа•Ла§В а§Ха•А ৙а§∞а§ња§≠а§Ња§Ја§Њ а§ѓа§Ьа•Ба§∞а•Н৵а•З৶ а§Ѓа•За§В а§єа•Иа•§ а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৪ড়৶а•Н৲ৌ৮а•Н১ а§Ѓа•За§В ৙а•Г৕а•Н৵а•А ১৕ৌ а§Єа•Ма§∞а§Ѓа§£а•На§°а§≤ а§Ха§Њ а§Жа§Ха§Ња§∞, а§Ч১ড় ুৌ৙ ১৕ৌ а§ѓа•Ба§Чুৌ৮ ৶ড়ৃৌ а§єа•Иа•§ а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓа§Ња§£а•На§° а§Ха§Њ а§Жа§Ха§Ња§∞ ৶ড়ৃৌ а§єа•Иа•§ а§За§Єа§Ха§Њ а§Єа•Га§Ја•На§Яа§њ ৪ড়৶а•Н৲ৌ৮а•Н১ ৙а•Ба§∞а•Ба§Ј а§Єа•Ва§Ха•Н১, а§Єа§Ња§Ва§Ца•На§ѓ ১৕ৌ ৙ৌа§Юа•На§Ъа§∞ৌ১а•На§∞ ৶а§∞а•Н৴৮ а§Ха§Њ ৪ু৮а•Н৵ৃ а§єа•Иа•§ а§ѓа§Ьа•Ба§∞а•Н৵а•З৶ ৵ৌа§Ь. а§Єа§В৺ড়১ৌ (а•Іа•Ђ/а•Іа•Ђ-а•Іа•ѓ, а•Іа•≠/а•Ђа•Ѓ, а•Іа•Ѓ/а•™а•¶) ১৕ৌ а§Ха•Ва§∞а•На§Ѓ ৙а•Ба§∞а§Ња§£ (а•™а•І/а•®-а•Ѓ), ু১а•На§Єа•На§ѓ ৙а•Ба§∞а§Ња§£ (а•Іа•®а•Ѓ/а•®а•ѓ-а•©а•©), а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓа§Ња§£а•На§° ৙а•Ба§∞а§Ња§£, а•І/а•®/а•®а•™-а•ђа•Ђ-а•≠а•©) а§Ж৶ড় а§Ѓа•За§В а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ а§∞৴а•На§Ѓа§ња§ѓа•Ла§В а§Ха•З а§Ѓа§Ња§Іа•На§ѓа§Ѓ а§ѓа§Њ а§Йа§Єа§Ха•А а§Ч১ড় а§Єа•З ু৮а•Ба§Ја•На§ѓ ৙а§∞ ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ ১৕ৌ а§Ча•На§∞а§є ৮а§Ха•Нৣ১а•На§∞а•Ла§В ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ а§Йа§Єа§Ѓа•За§В ৙а§∞ড়৵а§∞а•Н১৮ а§Ха§Њ ৵а§∞а•На§£а§® а§єа•Иа•§ а§ѓа§є ু৮а•Ба§Ја•На§ѓ а§Ха•Л ৵ড়৴а•Н৵ а§Ха•А ৙а•На§∞১ড়ুৌ а§∞а•В৙ а§Ѓа•За§В ৵а§∞а•На§£а§® а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§В, а§Ьа•Л ৵а•З৶ а§Ха§Њ а§Жа§Іа§Ња§∞ а§єа•Иа•§ а§Хড়৮а•Н১а•Б а§За§Єа§Ха•А ৵а•На§ѓа§Ња§Ца•На§ѓа§Њ а§Єа§Ѓа•Н৐৮а•На§Іа•А ৵а•З৶ৌа§Ща•На§Ч а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ а§Ча•На§∞৮а•Н৕ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§ѓа§є а§єа•Ла§∞а§Њ а§Ха§Њ ৵ড়ৣৃ а§єа•И а§Ьа§ња§Є ৙а§∞ ৙а§∞ৌ৴а§∞ ১৕ৌ ৵а§∞а§Ња§єа§Ѓа§ња§єа§ња§∞ а§Ха•А ৙а•На§∞а§Ња§Ъа•А৮ ৙а•Ба§Єа•Н১а§Ха•За§В а§єа•Иа§Ва•§ а§ѓа•З а§Єа§≠а•А ৵а•З৶ৌа§Ща•На§Ч а§єа•Иа§Ва•§
৵а•И৶ড়а§Х ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч
-৵а•З৶ а§Ѓа•За§В ৵ৌа§∞ ১৕ৌ ৵ৌ৪а§∞ ৶а•Л৮а•Ла§В ৴৐а•Н৶а•Ла§В а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч а§єа•Иа•§ ৵ৌ৪а§∞ а§Ха§Њ а§Єа•Н৙ৣа•На§Я а§Еа§∞а•Н৕ ৶ড়৮ а§єа•И а§Ьа•Л а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ а§Ха•З а§Й৶ৃ а§Єа•З а§Жа§∞а§Ѓа•На§≠ а§єа•Л১ৌ а§єа•И- а§Ж৶а•Н а§З১а•Н ৙а•На§∞১а•Н৮৪а•На§ѓ а§∞а•З১৪а§Г а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣа•Н৙৴а•Нৃ৮а•Н১ড় ৵ৌ৪а§∞а§Ѓа•На•§ ৙а§∞а•Л ৃ৶ড়৲а•Нৃ১а•З а§¶а§ња§µа§Ња•• (а§Ла§Ха•Н. а•Ѓ/а•ђ/а•©а•¶, ৪ৌু৵а•З৶ а•І/а•®а•¶, а§Ха§Ња§£а•Н৵ а§Єа§В. а•®/а•Іа•™, а§Р১а§∞а•За§ѓ а§Жа§∞а§£а•На§ѓа§Х, а•©/а•®/а•™а•Ѓ, а§Ыৌ৮а•Н৶а•Ла§Ча•На§ѓ а§Й৙৮ড়ৣ৶а•Н, а•©/а•Іа•≠/а•≠) а§Єа•Ла§Ѓ а§∞а§Ња§Ь৮а•Н ৙а•На§∞ а§£ а§Жа§ѓа•Ва§Ва§Ја§њ ১ৌа§∞а•Аа§Га•§ а§Е৺ৌ৮а•А৵ а§Єа•Ва§∞а•На§ѓа•Л ৵ৌ৪а§∞а§Ња§£а§ња•§ (а§Ла§Ха•Н, а•Ѓ/а•™а•Ѓ/а•≠, ৮ড়а§∞а•Ба§Ха•Н১,а•™/а•≠) ৵ৌа§∞ а§ѓа§Њ ৵ৌа§Г а§Ха•З а§Е৮а•На§ѓ а§Еа§∞а•Н৕ а§≠а•А а§єа•Иа§Ва•§ ৵ৌа§Г а§ѓа§Њ ৵ৌа§∞а•Н а§Ха§Њ а§Еа§∞а•Н৕ а§Ьа§≤ а§єа•И а§Ьа•Л а§Єа§ђа§Ха•Л а§Е৙৮а•З а§Ѓа•За§В а§∞а§Ц а§≤а•З১ৌ а§єа•И (а§Е৵ৌ৙а•Н৮а•Л১ড়, а§Ча•Л৙৕ а§ђа•На§∞а§Ња§єа•На§Ѓа§£, ৙а•Ва§∞а•Н৵, а•І/а•І/а•®-১৶а•Нৃ৶৐а•На§∞৵а•А৶ৌа§≠а§ња§∞а•Н৵ৌ а§Е৺ুড়৶а§В а§Єа§∞а•Н৵ুৌ৙а•На§Єа•На§ѓа§Ња§Ѓа§њ ৃ৶ড়৶а§В а§Ха§ња§Юа•На§Ъа•З১ড় ১৪а•Нুৌ৶ৌ৙а•Л а§ља§≠৵а§Ва§Єа•Н১৶৙ৌু৙а•Н১а•Н৵ুৌ৙а•Н৮а•Л১ড়)а•§ а§Ха•Ба§Ы а§Єа•Н৕а§≤а•Ла§В ৙а§∞ а§За§Єа§Ха§Њ а§Еа§∞а•Н৕ ৶ড়৮ а§Ха•На§∞а§Ѓ а§≠а•А а§єа•Л а§Єа§Х১ৌ а§єа•И, а§Ьа•Л а§ђа§Ња§∞-а§ђа§Ња§∞ а§Ж১ৌ а§єа•Иа•§ а§Е৴а•Н৵а•На§ѓа•Л ৵ৌа§∞а•Л а§Еа§≠৵৪а•Н১৶ড়৮а•Н৶а•На§∞ а§Єа•Га§Ха•З ৃ১а•Н১а•Н৵ৌ ৙а•На§∞১а•Нৃ৺৮а•Н ৶а•З৵ а§Па§Ха•§ а§Еа§Ьа§ѓа•Л а§Ча§Њ а§Еа§Ьа§ѓа§Г ৴а•Ва§∞ а§Єа•На§Єа•Лুু৵ৌ৪а•Га§Ьа§Г а§Єа§∞а•Н১৵а•З ৪৙а•Н১ ৪ড়৮а•На§Іа•В৮а•На•• (а§Ла§Ха•Н, а•І/а•©а•®/а•Іа•®) а§ѓа§єа§Ња§В ৙а•На§∞১ড় а§Еа§єа§Г (৶ড়৮) а§Ѓа•За§В а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৶а•З৵ (৶а•З৵ = а§Ьа•Л ৙а•На§∞а§Хৌ৴ড়১ а§Ха§∞а•З) а§Ха•З а§Й৶ৃ а§Єа•З ৵ৌа§∞ а§Ха§Њ ৮ড়а§∞а•Н৶а•З৴ а§єа•Иа•§ ৵ড়৴а•Н৵৪а•На§Ѓа§Њ а§З৶ড়ৣа•Ба§Іа•Нৃ১а•З ৶а•З৵১а•На§∞а§Њ ৺৵а•На§ѓа§Ѓа•Ла§єа§ња§Ја•За•§ ৵ড়৴а•Н৵৪а•На§Ѓа§Њ а§З১а•Н а§Єа•Ба§Ха•Г১а•З ৵ৌа§∞а§Ѓа•Га§£а•Н৵১а•На§ѓа§Ча•Н৮ড়а§∞а•Н৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ ৵а•На§ѓа•Га§£а•На§µа§§а§ња•• (а§Ла§Ха•Н, а•І/а•Іа•®а•Ѓ/а•ђ) а§ѓа§єа§Ња§В а§Па§Х ৵ৌа§∞ а§Ха•З ৪ুৌ৙а•Н১ а§єа•Л৮а•З ৙а§∞ а§Е৮а•На§ѓ ৵ৌа§∞ а§Ха•З а§Й১а•Н৙৮а•Н৮ а§єа•Л৮а•З а§Ха§Њ ৮ড়а§∞а•Н৶а•З৴ а§єа•Иа•§ ৵ড়৴а•Н৵৪а•На§Ѓа•И а§Єа•Ба§Ха•Г১а•З ৵ৌа§∞а§В а§Ла§£а•Н৵১ড়, ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ ৵ড়-а§Ла§£а•На§µа§§а§ња•§ ৵ড়৴а•Н৵৪а•На§Ѓа•И = а§Єа§ђа§Ха•З а§≤а§ња§Па•§ а§Єа•Ба§Ха•Г১ -৵ড়৴а•Н৵ а§Єа•Га§Ја•На§Яа§њ, а§Ьа§ња§Єа§Ѓа•За§В, а§Ха§∞а•Н১ৌ, а§Ха§∞а•На§Ѓ, а§Ђа§≤ а§Ж৶ড় а§Єа§≠а•А а§Па§Х а§єа•А а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓ а§єа•Иа§В( ১а•И১а•Н১ড়а§∞а•Аа§ѓ а§Й৙৮ড়ৣ৶а•Н, а•®/а•≠) ৵ৌа§∞ а•≠ а§єа•Л৮а•З а§Ха§Њ а§Жа§Іа§Ња§∞ а§єа•И-а•≠ ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•З а§Ъа§Ха•На§∞а•§ а§Єа•Т৙а•Н১ৌ৪а•На§ѓа§Ња•С৪৮а•Н৙а§∞а§ња•Та§Іа§ѓа•Та§Єа•Н১а•На§∞а§ња§Г а§Єа•Т৙а•Н১ а§Єа•Та§Ѓа§ња§Іа§Га•С а§Ха•Га•Т১ৌа§Га•§ ৶а•За•Т৵ৌ ৃ৶а•На§ѓа•Та§Ьа•На§Ю৮а•Н১а•С৮а•Н৵ৌа•Т৮ৌ৚а§Еа§ђа•Са§Іа•Н৮а•Т৮а•Н৙а•Ба§∞а•Ба•Са§Ја§Ѓа•Н৙а•Т৴а•Ба§Ѓа•На••а•Іа•Ђа•• (৙а•Ба§∞а•Ба§Ј а§Єа•Ва§Ха•Н১, ৵ৌа§Ь. а§Єа§В. а•©а•І/а•Іа•Ђ) а§ѓа§єа§Ња§В а§ѓа§Ьа•На§Ю а§Ха•З а§≤а§ња§П а•™ ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•З ৪৙а•Н১ а§єа•Иа§В-১а•На§∞а§њ-৪৙а•Н১ а§Єа§Ѓа§ња§Іа§Њ, ৪৙а•Н১ ৙а§∞а§ња§Іа§ња•§ а§Єа§Ѓа§ња§Іа§Њ а§Ха§Њ а§Еа§∞а•Н৕ а§ѓа§Ьа•На§Ю а§Ха•А а§Єа§Ња§Ѓа§Ча•На§∞а•Аа•§ ৙а§∞а§ња§Іа§њ а§Ха•З а§Ха§И а§Еа§∞а•Н৕ а§єа•Иа§В-а•≠ а§≤а•Ла§Х, а§Ьа•Л ৙а§∞а§ња§Іа§њ а§Ха•З а§≠а•А১а§∞ а§Єа•Аুড়১ а§єа•Иа§В, а§Ха§Ња§≤ а§Ъа§Ха•На§∞ а§Ѓа•За§В а•≠ ৙а•На§∞а§Ха§Ња§∞ а§Ха•З а§ѓа•Ба§Ч, а§ѓа§Њ а§Йа§Єа§Ха•А ৙а•На§∞১ড়ুৌ а§∞а•В৙ а•≠ ৵ৌа§∞ а§Ха•З а§Ъа§Ха•На§∞а•§ ৪৙а•Н১ а§ѓа•Ба§Юа•На§Ь৮а•Н১ড় а§∞৕ুа•За§Х а§Ъа§Ха•На§∞а•Л а§Па§Ха•Л а§Е৴а•Н৵а•Л ৵৺১ড় ৪৙а•Н১৮ৌুৌ-(а§Еа§Єа•На§ѓ ৵ৌুа•Аа§ѓ а§Єа•Ва§Ха•Н১, а§Ла§Ха•Н, а•І/а•Іа•ђа•™/а•®) а§Ха§Ња§≤ ৙а•На§∞৵ৌ৺ а§Ха•Л а§єа•А а§Е৴а•Н৵ а§Ха§єа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•И- а§Ха§Ња§≤а•Л а§Е৴а•Н৵а•Л ৵৺১ড় ৪৙а•Н১а§∞৴а•На§Ѓа§ња§Г а§Єа§єа§Єа•На§∞а§Ња§Ха•На§Ја•Л а§Еа§Ьа§∞а•Л а§≠а•Ва§∞а§ња§∞а•З১ৌа§Га•§ ১ুৌа§∞а•Л৺৮а•Н১ড় а§Х৵ৃа•Л ৵ড়৙৴а•На§Ъড়১৪а•Н১৪а•На§ѓ а§Ъа§Ха•На§∞а§Њ а§≠а•Б৵৮ৌ৮ড় ৵ড়৴а•На§µа§Ња••а•Іа•• ৪৙а•Н১ а§Ъа§Ха•На§∞ৌ৮а•Н ৵৺১ড় а§Ха§Ња§≤ а§Па§Ј ৪৙а•Н১ৌ৪а•На§ѓ ৮ৌа§≠а•Аа§∞а§Ѓа•Г১а§В ৮а•Н৵а§Ха•На§Ја§Га•§ а§Єа§Њ а§За§Ѓа§Њ ৵ড়৴а•Н৵ৌ а§≠а•Б৵৮ৌ৮а•На§ѓа§Юа•На§Ь১а•Н а§Ха§Ња§≤а§Г а§Є а§Иৣ১а•З ৙а•На§∞৕ুа•Л ৮а•Б ৶а•З৵а§Га••а•®а•• (а§Е৕а§∞а•Н৵, ৴а•М৮а§Х, а•Іа•ѓ/а•Ђа•©) а§Е৴а•Н৵ а§Ха§Њ а§Еа§∞а•Н৕ а§єа•И а§Ч১ড় а§Ха§Њ а§Єа§Ња§Іа§®а•§ а§Ч১ড় а§ѓа§Њ ৙а§∞ড়৵а§∞а•Н১৮ а§Єа•З а§Ха§Ња§≤ а§Ха§Њ а§Ьа•На§Юৌ৮ ১৕ৌ а§Йа§Єа§Ха•А ুৌ৙ а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§ а§∞а•В৙ৌ৮а•Н১а§∞а§В ১৶а•Н ৶а•Н৵ড়а§Ь а§Ха§Ња§≤а§Єа§Ва§Ьа•На§Юа§Ѓа•Н (৵ড়ৣа•На§£а•Б ৙а•Ба§∞а§Ња§£, а•®/а•®/а•®а•™) а§Ч১ড় а§ѓа§Њ а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ а§Єа•З а§ѓа§Ьа•На§Ю а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ а§ѓа§Ьа•На§Ю а§Єа•З ৮ড়а§∞а•Нুড়১ ৙৶ৌа§∞а•Н৕ а§Ла§Ха•Н а§ѓа§Њ а§Ѓа•Ва§∞а•Н১ড় а§∞а•В৙ а§єа•Иа•§ а§Ха§Ња§≤ а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ ৮ড়а§∞а•На§Ѓа§Ња§£ а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ а§ѓа§Ьа•На§Ю а§єа•Иа•§ а§™а§ња§£а•На§° а§ѓа§Њ ৶а•Г৴а•На§ѓ а§Ьৌ১а•Н а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§Ла§Ха•Н ৙а•На§∞৕ু ৵а•З৶ а§єа•Иа•§ а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ а§ѓа§Њ а§ѓа§Ьа•На§Ю а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§ѓа§Ьа•Ба§∞а•Н৵а•З৶ а§Ѓа•Ба§Ца•На§ѓ а§єа•Иа•§ а§Ьа•На§Юৌ৮ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§Єа§Ња§Ѓ а§Ѓа•Ба§Ца•На§ѓ а§єа•И, а§єа§Ѓ ১а§Х а§Ха§ња§Єа•А ৵৪а•Н১а•Б а§Ха§Њ а§Єа§Ња§Ѓ а§ѓа§Њ ৙а•На§∞а§≠ৌ৵ ৙৺а•Ба§Ва§Ъ৮а•З ৙а§∞ а§Йа§Єа§Ха§Њ а§Ьа•На§Юৌ৮ а§єа•Л১ৌ а§єа•И (৵а•З৶ৌ৮ৌа§В ৪ৌু৵а•З৶а•Ла§ља§Єа•На§Ѓа§њ-а§Ча•А১ৌ, а•Іа•¶/а•®а•®)а•§ а§Ха§Ња§≤а•Л а§є а§≠а•В১ а§≠৵а•На§ѓа§В а§Ъ ৙а•Б১а•На§∞а•Л а§Еа§Ь৮ৃ১а•Н ৙а•Ба§∞а§Ња•§ а§Ха§Ња§≤ৌ৶а•Га§Ъа§Г а§Єа§Ѓа§≠৵৮а•Н а§ѓа§Ьа•Ба§Г а§Ха§Ња§≤ৌ৶а§Ьа§Ња§ѓа§§а••а•©а•• а§Ха§Ња§≤а•Л а§ѓа§Ьа•На§Юа§В а§Єа§Ѓа•Иа§∞৶а•Н ৶а•З৵а•За§≠а•На§ѓа•Л а§≠а§Ња§Ча§Ѓа§Ха•Нৣড়১ুа•На•§ а§Ха§Ња§≤а•З а§Ч৮а•На§Іа§∞а•Н৵ৌ৙а•На§Єа§∞а§Єа§Г а§Ха§Ња§≤а•З а§≤а•Ла§Ха§Ња§Г ৙а•На§∞১ড়ৣа•Н৆ড়১ৌа§Га••а•™а•• а§За§Ѓа§В а§Ъ а§≤а•Ла§Ха§В ৙а§∞а§Ѓа§В а§Ъ а§≤а•Ла§Ха§В ৙а•Ба§£а•На§ѓа§Ња§В৴а•На§Ъ а§≤а•Ла§Хৌ৮а•Н ৵ড়৲ড়১ড়৴а•На§Ъ ৙а•Ба§£а•На§ѓа§Ња§Га•§ а§Єа§∞а•Н৵ৌа§Ва§≤а•На§≤а•Ла§Хৌ৮а§≠а§ња§Ьড়১а•На§ѓ а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓа§£а§Њ а§Ха§Ња§≤а§Г а§Є а§Иৃ১а•З ৙а§∞а§Ѓа•Л ৮а•Б ৶а•З৵а§Га••а•Ђа•• (а§Е৕а§∞а•Н৵, ৴а•М৮а§Х, а•Іа•ѓ/а•Ђа•™) а§Ха§Ња§≤ а§Ча§£а§®а§Њ а§Ха§Њ а§ѓа§є а§∞а•В৙ а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓа§Њ ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ ৮ড়а§∞а•На§Іа§Ња§∞ড়১ а§єа•Ба§Ж а§Ьа§ђ а§Еа§≠а§ња§Ьড়১а•Н ৮а§Ха•Нৣ১а•На§∞ а§Ха•А ৶ড়৴ৌ а§Ѓа•За§В а§Іа•На§∞а•Б৵ ৕ৌ (а•©а•Ѓ,а•¶а•¶а•¶ а§И৙а•В)а•§ а§Йа§Є а§Єа§Ѓа§ѓ а§Еа§≠а§ња§Ьড়১а•Н а§Єа•З ৵а§∞а•На§Ј а§Жа§∞а§Ѓа•На§≠ а§єа•Л১ৌ а§•а§Ња•§ ৐ৌ৶ а§Ѓа•За§В а§Ха§Ња§∞а•Н১а•Н১ড়а§Ха•За§ѓ а§Ха•З а§Єа§Ѓа§ѓ а§Єа•З а§Еа§≠а§ња§Ьড়১а•Н а§Ха§Њ ৙১৮ а§єа•Л৮а•З ৙а§∞ ৲৮ড়ৣа•Н৆ৌ а§Єа•З ৵а§∞а•На§Ј ১৕ৌ ৵а§∞а•На§Ја§Њ а§Ха§Њ а§Жа§∞а§Ѓа•На§≠ а§єа•Ба§Ж (а§Ѓа§єа§Ња§≠а§Ња§∞১, ৵৮ ৙а§∞а•Н৵, а•®а•©а•¶/а•Ѓ-а•Іа•¶)
৵ৌа§∞ а§Ха•А а§Ж৵৴а•На§ѓа§Х১ৌ
-а§Р১ড়৺ৌ৪ড়а§Х а§Ха§Ња§≤а§Ха•На§∞а§Ѓ а§ѓа§Њ а§Ша§Я৮ৌ а§Ха§Њ ৵а§∞а•На§£а§® а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П ৵ৌа§∞ а§Ха•А а§Ж৵৴а•На§ѓа§Х১ৌ ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§Е১а§Г а§З১ড়৺ৌ৪ а§Ча•На§∞৮а•Н৕а•Ла§В а§Ѓа•За§В а§За§Єа§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৪ড়৶а•Н৲ৌ৮а•Н১ а§Ѓа•За§В а§Ха§ња§Єа•А ৮ড়а§∞а•Н৶ড়ৣа•На§Я а§Ха§Ња§≤ а§Єа•З ৶ড়৮ а§Єа§Ѓа•Ва§є (а§Еа§єа§∞а•На§Ча§£) а§Ха•А а§Ча§£а§®а§Њ а§Ѓа•За§В ৵ৌа§∞ а§Ха•А а§Ж৵৴а•На§ѓа§Х১ৌ а§єа•Иа•§ а§Єа•Ма§∞ ৵а§∞а•На§Ј а§Ѓа•За§В а§Ха•На§∞а§Ѓа§Ња§Ч১ ৶ড়৮а•Ла§В а§Ха•А а§Ча§£а§®а§Њ а§єа•Л১а•А а§єа•И, а§Йа§Єа§Ѓа•За§В а§≠а•А а§Л১а•Б৴а•За§Ј ৮ড়а§Ха§Ња§≤৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П ৶ড়৮а•Ла§В а§Ха§Њ а§Ьа•Ла•Ь а§Ша§Яৌ৵ а§Ха§∞৮ৌ ৙а•Ь১ৌ а§єа•Иа•§ а§Ъৌ৶а•На§∞ а§Ѓа§Ња§Є а§Ха§Њ ৪ু৮а•Н৵ৃ а§Ха§∞৮а•З а§Ха•З а§≤а§ња§П а§≤а§Ѓа•На§ђа•А а§Ча§£а§®а§Њ а§єа•Иа•§ а§Ъৌ৮а•Н৶а•На§∞ ১ড়৕ড়, а§Ѓа§Ња§Є, ৵а§∞а•На§Ј а§Ха§Њ а§Ха•На§∞а§Ѓа§Ња§Ч১ ৶ড়৮а•Ла§В, а§Єа•Ма§∞ а§Ѓа§Ња§Є а§ѓа§Њ ৵а§∞а•На§Ј а§Єа•З а§Єа•Н৙ৣа•На§Я а§Єа§Ѓа•Н৐৮а•На§І ৮৺а•Аа§В а§єа•И ১৕ৌ ৵৺ ৐৶а§≤১ৌ а§∞৺১ৌ а§єа•Иа•§ а§Йа§Єа§Ха•А ৴а•Б৶а•На§Іа§њ а§Ха•З а§≤а§ња§П ৶а•За§Ца§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И а§Ха§њ ৶ড়৮ а§Єа§Ва§Ца•На§ѓа§Њ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞а§Жа§Ь а§Ьа•Л ৵ৌа§∞ а§Ж а§∞а§єа§Њ а§єа•И, ৵৺ ৆а•Аа§Х а§єа•И а§ѓа§Њ ৮৺а•Аа§Ва•§ а§Е৴а•Б৶а•На§Іа§њ а§єа•Л৮а•З ৙а§∞ а•І-а•® ৶ড়৮ а§Ха§Ѓ а§ѓа§Њ а§Еа§Іа§ња§Х а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§За§Єа•З ৵ৌа§∞ ৴а•Б৶а•На§Іа§њ а§Х৺১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Жа§Іа•Б৮ড়а§Х а§Ьа•На§ѓа•Л১ড়ৣ а§Ѓа•За§В а§≠а•А ৙а•На§∞а§Ња§Ъа•А৮ а§Ча§£а§®а§Ња§Ха•З а§≤а§ња§П а§Па§Х а§Ха§Ња§≤а•Н৙৮ড়а§Х а§Жа§Іа§Ња§∞ а§≤а§ња§ѓа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§єа•И-а•І-а•І-а•™а•≠а•Іа•© а§И৙а•В, а§Ьа§ња§Є ৶ড়৮ ৴а•Ба§Ха•На§∞৵ৌа§∞ а§•а§Ња•§ а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৪ড়৶а•Н৲ৌ৮а•Н১ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§Єа•Га§Ја•На§Яа•Нৃৌ৶ড় а§Еа§єа§∞а•На§Ча§£ а§Ха•З а§≤а§ња§П а§∞৵ড়৵ৌа§∞ а§Єа•З ৵ৌа§∞ а§Жа§∞а§Ѓа•На§≠ а§Ха§∞১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Єа§Ѓа•На§≠৵১а§Г ৙а•Ва§∞а•З ৵ড়৴а•Н৵ а§Ѓа•За§В а§ѓа§є а§Єа•Н৵а•Аа§Ха•Г১ ৕ৌ а§Е১а§Г а§∞৵ড়৵ৌа§∞ а§Ха•А а§Ыа•Ба§Яа•На§Яа•А а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§Ъа§≤৮ а§єа•Ба§Жа•§ а§ђа§Ња§За§ђа§ња§≤ а§Ха•З а§Жа§∞а§Ѓа•На§≠ а§Ѓа•За§В а§Єа•Га§Ја•На§Яа§њ а§Ха§Њ ৪৙а•Н১ু ৶ড়৮ (ু৮а•Н৵৮а•Н১а§∞) а§Ъа§≤ а§∞а§єа§Њ а§єа•Иа•§ а§Ха§≤а§њ а§Жа§∞а§Ѓа•На§≠ а§Єа•З а§Ча§£а§®а§Њ а§Ха•З а§≤а§ња§П ৙а•На§∞৕ু ৵ৌа§∞ а§ђа•Б৲৵ৌа§∞ ুৌ৮১а•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৪ড়৶а•Н৲ৌ৮а•Н১ а§Ха•З ৙а•Ва§∞а•Н৵ а§ђа•На§∞а§єа•На§Ѓа§Њ ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ а§Еа§≠а§ња§Ьড়১а•Н а§Єа•З а§ѓа§Њ а•Іа•Ђа•Ѓа•¶а•¶ а§И৙а•В а§Ѓа•За§В а§Ха§Ња§∞а•Н১а•Н১ড়а§Ха•За§ѓ ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ ৲৮ড়ৣа•Н৆ৌ а§Єа•З ৵а§∞а•На§Ј а§Жа§∞а§Ѓа•На§≠ а§єа•Л৮а•З ৙а§∞ ৵а§∞а•На§Ј а§Ха§Њ ৙а•На§∞৕ু а§Ѓа§Ња§Є а§Ѓа§Ња§Ш а§єа•Л১ৌ а§•а§Ња•§ а§ѓа§є а§≠а•А а§Ъৌ৮а•Н৶а•На§∞ а§Ѓа§Ња§Є ৕ৌ а§Ьа§ња§Єа§Ѓа•За§В ৙а•Ва§∞а•На§£а§ња§Ѓа§Њ а§Ха•З а§Ъৌ৮а•Н৶а•На§∞ ৮а§Ха•Нৣ১а•На§∞ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§Ѓа§Ња§Є ৮ৌু а§єа•Л১ৌ а§•а§Ња•§ а§Е১а§Г а§Йа§Є а§Єа§Ѓа§ѓ а§Ха•А а§Ха§Ња§≤ а§Ча§£а§®а§Њ ৐ড়৮ৌ ৵ৌа§∞ ৴а•Б৶а•На§Іа§њ а§Ха•З а§Єа§Ѓа•На§≠৵ ৮৺а•Аа§В ৕а•Аа•§ ৵ৌа§∞ а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч а§Ѓа•Ба§єа•Ва§∞а•Н১а•Н১ ৮ড়а§∞а•На§£а§ѓ а§ѓа§Њ ৪ৌ৙а•Н১ৌ৺ড়а§Х ৶ড়৮а§Ъа§∞а•На§ѓа§Њ, ৴ড়а§Ха•На§Ја§Њ а§Ха§Њ а§Ха§Ња§∞а•На§ѓа§Ха•На§∞а§Ѓ (а§∞а•Ба§Яа•А৮) а§Ж৶ড় а§Ха•З а§≤а§ња§П а§єа•Иа•§ ৵ৌа§∞ а§Ха•На§∞а§Ѓ
-а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৪ড়৶а•Н৲ৌ৮а•Н১, а§≠а•Ва§Ча•Ла§≤ а§Еа§Іа•На§ѓа§Ња§ѓ (а•≠а•Ѓ), а§Жа§∞а•На§ѓа§≠а§Яа•Аа§ѓ а§Ха•З а§Ха§Ња§≤а§Ха•На§∞а§ња§ѓа§Њ ৙ৌ৶ (а•Іа•ђ) а§Ѓа•За§В ৵ৌа§∞ а§Ха•На§∞а§Ѓ а§Ха§Њ а§Жа§Іа§Ња§∞ ৶ড়ৃৌ а§єа•Иа•§ ু৮а•Н৶ а§Ч১ড় а§Єа•З а§Ха•На§∞ু৴а§Г ১а•А৵а•На§∞ а§Ч১ড় а§Ха•З а§Ча•На§∞а§є а§єа•Иа§В-৴৮ড়, а§ђа•Га§єа§Єа•Н৙১ড়, а§Ѓа§Ва§Ча§≤, а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ (৙а•Г৕а•Н৵а•А), ৴а•Ба§Ха•На§∞, а§ђа•Ба§І, а§Ъ৮а•Н৶а•На§∞а•§ ৙а•На§∞১ড়৶ড়৮ ৙а•Ва§∞а•Н৵ а§Ха•Нৣড়১ড়а§Ь ৙а§∞ а•Іа•® а§∞ৌ৴ড়ৃа•Ла§В а§Ха§Њ а§Ха•На§∞а§Ѓа§Ња§Ч১ а§Й৶ৃ а§єа•Л১ৌ а§єа•И а§Ьа§ња§Єа•З а§Йа§Є а§Єа•Н৕ৌ৮ а§Ха§Њ а§≤а§Ча•Н৮ а§Х৺১а•З а§єа•Иа§Ва•§ ৙а•На§∞১а•На§ѓа•За§Х а§∞ৌ৴ড় а§Ха§Њ а§Жа§Іа§Њ а§≠а§Ња§Ч а§єа•Ла§∞а§Њ (а§Еа§єа•Л-а§∞ৌ১а•На§∞ а§Ха§Њ а§Ха•З а§Ѓа§Іа•На§ѓ а§Еа§Ха•На§Ја§∞) а§єа•Иа•§ а§Е১а§Г ৙а•На§∞১ড়৶ড়৮ а•®а•™ а§єа•Ла§∞а§Њ а§Ха§Њ а§Й৶ৃ а§єа•Л১ৌ а§єа•Иа•§ а§єа•Ла§∞а§Њ а§Єа•З а§Еа§Ва§Ча•На§∞а•За§Ьа•А а§Ѓа•За§В а§Ж৵а§∞ (hour) а§єа•Ба§Ж а§єа•Иа•§ а§Ха§ња§Єа•А ৵ৌа§∞ а§Ха•А ৙а•На§∞৕ু а§єа•Ла§∞а§Њ а§Йа§Єа•А а§Ча•На§∞а§є а§Ха•А а§єа•Л১а•А а§єа•Иа•§ а§Йа§Єа§Ха•З ৐ৌ৶ а§ђа•Э১а•А а§Ч১ড় а§Ха•З а§Ха•На§∞а§Ѓ а§Єа•З а§Е৮а•На§ѓ а§Ча•На§∞а§єа•Ла§В а§Ха•А а§єа•Ла§∞а§Њ а§єа•Ла§Ча•Аа•§ ৃ৕ৌ ৴৮ড় ৵ৌа§∞ а§Ха•Л ৙а•На§∞৕ু а§єа•Ла§∞а§Њ ৴৮ড় а§Ча•На§∞а§є а§Ха•А а§єа•Ла§Ча•Аа•§ а§Йа§Єа§Ха•З ৐ৌ৶ а•®а•І а§єа•Ла§∞а§Њ ১а§Х а•≠ а§Ча•На§∞а§єа•Ла§В а§Ха§Њ а•© а§Ъа§Ха•На§∞ ৙а•Ва§∞а§Њ а§єа•Л а§Ьа§Ња§ѓа•За§Ча§Ња•§ ৶ড়৮ а§∞а•В৙а•А а§Єа§Ѓа§ња§Іа§Њ а§≠а•А ১а•На§∞а§њ-৪৙а•Н১ а§єа•Иа•§ а§Йа§Єа§Ха•З ৐ৌ৶ а§Йа§Є ৶ড়৮ а§Ха•А а•© а§єа•Ла§∞а§Њ ১৕ৌ а§Еа§Ча§≤а•З ৶ড়৮ а§Ха•А ৙а•На§∞৕ু а§єа•Ла§∞а§Њ а§Жа§ѓа•За§Ча•Аа•§ а§З৮а§Ха•А а§Чড়৮১а•А ৙а•Б৮а§Г ৴৮ড় а§Єа•З а§єа•Ла§Ча•А-৴৮ড়, а§ђа•Га§єа§Єа•Н৙১ড়, а§Ѓа§Ва§Ча§≤, а§Єа•Ва§∞а•На§ѓа•§ а§Е১а§Г а§Еа§Ча§≤а§Њ ৶ড়৮ а§∞৵ড়৵ৌа§∞ а§єа•Ла§Ча§Ња•§ а§Єа•Ва§∞а•На§ѓ ৪ড়৶а•Н৲ৌ৮а•Н১ а§Ха§Њ ৵а§∞а•Н১ুৌ৮ а§∞а•В৙ а§Ѓа§ѓа§Ња§Єа•Ба§∞ ৶а•Н৵ৌа§∞а§Њ а§Єа§В৴а•Л৲ড়১ а§єа•И (а•ѓа•®а•®а•© а§И৙а•В) а§Ѓа•За§Ва•§ а§За§Єа§Ѓа•За§В ৙а•Г৕а•Н৵а•А а§Еа§Ха•На§Ј а§Ха§Њ а§Эа•Ба§Хৌ৵, ৶ড়৮-৵а§∞а•На§Ј а§Ха§Њ а§Е৮а•Б৙ৌ১ а§Ж৶ড় а§Йа§Єа•А а§Ха§Ња§≤ а§Ха•З а§єа•Иа§Ва•§ а§Е১а§Г а§Ха§Ѓ а§Єа•З а§Ха§Ѓ а•Іа•І,а•¶а•¶а•¶ ৵а§∞а•На§Ј а§Єа•З ৵ৌа§∞ ৙а•На§∞৵а•Г১а•Н১ড় а§Ъа§≤ а§∞а§єа•А а§єа•Иа•§
৙а•На§∞а§Ња§ѓа§Г а§ѓа§є а§Ха§єа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§≠а§Ња§∞১ а§Ѓа•За§В ৵ৌа§∞ а§Ха§Њ ৙а•На§∞а§Ъа§≤৮ ৮৺а•Аа§В ৕ৌ, а§ѓа§є а§Єа•Ба§Ѓа•За§∞а§ња§ѓа§Њ а§Єа•З а§Жа§ѓа§Њ а§•а§Ња•§ а•ђа•¶ ৵а§∞а•На§Ј а§Ха•З а§Ъа§Ха•На§∞ а§Ха•Л а§≠а•А а§Х৺১а•З а§єа•Иа§В а§Ха§њ а§ѓа§є а§Єа•Ба§Ѓа•За§∞а§ња§ѓа§Њ а§Єа•З а§Жа§ѓа§Њ а§•а§Ња•§ а§Еа§≠а•А ১а§Х а§Єа•Ба§Ѓа•За§∞а§ња§ѓа§Њ а§Ха•А а§Ха•Ла§И а§Ра§Єа•А ৙а•Ба§Єа•Н১а§Х ৮৺а•Аа§В а§Ѓа§ња§≤а•А а§єа•И а§Ьа§ња§Єа§Ѓа•За§В ৵ৌа§∞ ৙а•На§∞৵а•Г১а•Н১ড় а§ѓа§Њ а•ђа•¶ ৵а§∞а•На§Ј а§Ха•З а§Ъа§Ха•На§∞ а§Ха§Њ ৵а§∞а•На§£а§® а§єа•Ла•§ ৃ৶ড় а§Ха§єа•За§В а§Ха§њ ৵ড়ৣа•На§£а•Б а§Іа§∞а•На§Ѓа•Л১а•Н১а§∞ ৙а•Ба§∞а§Ња§£ а§Ѓа•За§В а•ђа•¶ ৵а§∞а•На§Ј а§Ха•З а§Ъа§Ха•На§∞ а§Ха§Њ ৵ড়৪а•Н১а•Г১ ৵а§∞а•На§£а§® а§єа•И, ১а•Л а§Йа§Єа§Ха§Њ а§Й১а•Н১а§∞ а§Ѓа§ња§≤১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§ѓа§є а•Іа•®а•¶а•¶ а§И а§Ха•З ৐ৌ৶ а§Ха•А а§∞а§Ъ৮ৌ а§єа•Иа•§ а§≠а§Ња§∞১ а§Ха•З а§Еа§Іа§ња§Ха§Ња§В৴ а§ђа•Б৶а•На§Іа§ња§Ьа•А৵ড়ৃа•Ла§В а§Ха§Њ ৵ড়৴а•Н৵ৌ৪ а§єа•И а§Ха§њ ৶ড়а§≤а•На§≤а•А ৙а§∞ а§Ѓа•Ба§Єа•На§≤а§ња§Ѓ а§Еа§Іа§ња§Ха§Ња§∞ а§єа•Л৮а•З а§Ха•З ৐ৌ৶ а§єа•А а§≠а§Ња§∞১ а§Ѓа•За§В ৙а•Ба§∞а§Ња§£ а§≤а§ња§Ца•З а§Ча§ѓа•За•§ а§Жа§∞а•На§ѓа§≠а§Я а§Ха§Њ а§Єа§Ѓа§ѓ а§Ца§ња§Єа§Ха§Њ а§Ха§∞ а§Ха§єа§Њ а§Ча§ѓа§Њ а§Ха§њ а§Й৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§Ча•На§∞а•Аа§Є а§Ха•З ৺ড়৙а•Н৙ৌа§∞а•На§Ха§Є а§Ха•А а§Ьа•На§ѓа§Њ а§Єа§Ња§∞а§£а•А а§Ха•А ৮а§Ха§≤ а§Ха•Аа•§ а§Па§Х а§ђа§Ња§∞ а§°а•З৵ড়ৰ ৙ড়а§Ва§Ча§∞а•А а§Єа•З а§Ѓа•Иа§В৮а•З ৙а•Ва§Ыа§Њ а§≠а•А ৕ৌ а§Ха§њ ৺ড়৙а•Н৙ৌа§∞а•На§Ха§Є а§Ха•А а§Ьа•На§ѓа§Њ а§Єа§Ња§∞а§£а§Њ а§Ха§єа§Ња§В а§єа•И ১а•Л а§Й৮а•На§єа•Ла§В৮а•З а§Ха§єа§Њ а§Ха§њ а§ѓа§є ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§Й৮а§Ха•Л а§Ха§єа§Њ а§Ха§њ а§Е৙৮а•З ু১ а§Ха•З а§Єа§Ѓа§∞а•Н৕৮ а§Ѓа•За§В а§Ха§Ѓ а§Єа•З а§Ха§Ѓ а§Еа§ђ ৺ড়৙а•Н৙ৌа§∞а•На§Ха§Є а§Ха•З ৮ৌু ৙а§∞ а§Ча•На§∞а•Аа§Х а§Ѓа•За§В а§Ьа•На§ѓа§Њ а§Єа§Ња§∞а§£а•А ৐৮ৌ ৶а•За§Ва•§ а§Й৮৺а•Ла§В৮а•З а§Ха§єа§Њ а§Ха§ња§Ча•На§∞а•Аа§Х ৮৺а•Аа§В а§Ж১а•А а§єа•Иа•§ а§Жа§∞а•На§ѓа§≠а§Я ৮а•З а§Ха§ња§Є ৵ড়৶а•На§ѓа§Ња§≤а§ѓ а§Ѓа•За§В а§Фа§∞ а§Ха•На§ѓа•Ла§В а§Ча•На§∞а•Аа§Х ৙а•Эа§Њ ৕ৌ? а§Ча•На§∞а•Аа§Х а§Ѓа•За§В а§Еа§Ва§Х а§Ха•А ৶৴ুа§≤৵ ৙৶а•Н৲১ড় ৮৺а•Аа§В ৕а•А, а§Е১а§Г а§Й৮а§Ха•А а§Єа§Ва§Ца•На§ѓа§Њ ৙৶а•Н৲১ড় а§Ѓа•За§В а§Ха•Ла§И а§Ча§£а§ња§§ а§Єа§Ња§∞а§£а•А ৮৺а•Аа§В ৐৮ а§Єа§Х১а•А а§єа•Иа•§ а§За§Є а§Ха§Ња§∞а§£ ৵৺ৌа§В а§Ча§£а§®а§Њ а§Єа§Ѓа•Н৐৮а•На§Іа•А а§Ха•Ла§И ৙а•Ба§Єа•Н১а§Х ৮৺а•Аа§В а§єа•Иа•§ а§Ха§єа§Њ а§Ьৌ১ৌ а§єа•И а§Ха§њ а§∞а§Ња§Ѓа§Ња§ѓа§£, а§Ѓа§єа§Ња§≠а§Ња§∞১ а§Ѓа•За§В а§Йа§≤а•На§≤а•За§Ц ৮৺а•Аа§В а§єа•И а§Е১а§Г а§≠а§Ња§∞১ а§Ѓа•За§В ৵ৌа§∞ а§Ха§Њ а§Йа§≤а•На§≤а•За§Ц ৮৺а•Аа§В а§•а§Ња•§ а§≠а§Ња§∞১ ৵ড়а§∞а•Б৶а•На§І ১а§∞а•На§Ха•Ла§В а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ ৃ৶ড় ৵ড়৴а•Н৵ а§З১ড়৺ৌ৪ а§Ха•А а§Єа§Ѓа•Аа§Ха•На§Ја§Њ а§єа•Л ১а•Л а§Еа§≠а•А ১а§Х ৵ড়৴а•Н৵ а§Ѓа•За§В а§Ха§єа•Аа§В а§≠а•А ৵ৌа§∞ ৙а•На§∞৵а•Г১а•Н১ড় а§Жа§∞а§Ѓа•На§≠ ৮৺а•Аа§В а§єа•Ба§И а§єа•Иа•§ а§Еа§Ѓа•За§∞а§ња§Ха§Њ а§Ха•З ৵а§∞а•Н১ুৌ৮ а§∞а§Ња§Ја•На§Яа•На§∞৙১ড় ৮а•З а•®а•¶ а§Ь৮৵а§∞а•А а§Ха•Л ৴৙৕ а§≤а•Аа•§ ৵৺ а§Ха•М৮ а§Єа§Њ ৵ৌа§∞ ৕ৌ а§ѓа§Њ ৵ৌа§∞ а§Ха•З а§Е৮а•Ба§Єа§Ња§∞ а§За§Є а§Єа§Ѓа§ѓ а§Ха§Њ ৮ড়а§∞а•На§£а§ѓ а§єа•Ба§Ж ৕ৌ? а§≠а§Ња§∞১ а•Іа•Ђа§Еа§Ча§Єа•Н১ а•Іа•ѓа•™а•≠ а§Ха•Л а§Єа•Н৵ৌ৲а•А৮ а§єа•Ба§Ж? а§Йа§Є ৶ড়৮ а§Ха•М৮ а§Єа§Њ ৵ৌа§∞ ৕ৌ ১৕ৌ а§ѓа§є а§Ха§ња§Є ৙а•Ба§Єа•Н১а§Х а§Ѓа•За§В а§≤а§ња§Ца§Њ а§єа•И? ৵ৌа§∞ а§Ха•З ৙а•На§∞а§ѓа•Ла§Ч а§Ха§єа§Ња§В ১৕ৌ а§Ха•На§ѓа•Ла§В а§єа•И, а§За§Єа§Ха•А а§Єа§Ѓа•Аа§Ха•На§Ја§Њ а§Ха•А а§Ьа§Њ а§∞а§єа•А а§єа•Иа•§
